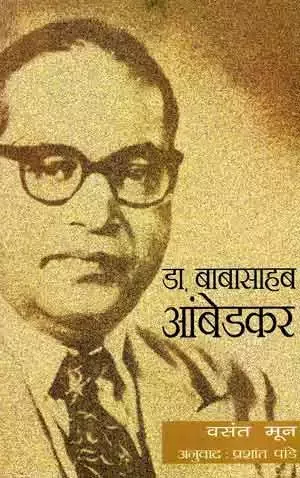|
जीवनी/आत्मकथा >> डा. बाबासाहब आंबेडकर डा. बाबासाहब आंबेडकरवसंत मनु
|
337 पाठक हैं |
|||||||
डा. बाबासाहब आंबेडकर के जीवन पर आधारित पुस्तक....
Dr. babasahab Ambedkar
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय संविधान के रचयिता डा. बाबासाहब आंबेड़कर केवल दलितों के ही नेता नहीं थे, जो धारणा जन मानस में फैली हुई है, वरन् वह एक ऐसे राष्ट्रपुरूष थे, जिन्होंने समूचे देश के संबंध में, भारत के इतिहास के संबंध में और समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया है। ड़ा. आंबेडकर एक विद्वान लेखक, विधिवेत्ता, राजनयिक, समाजसुधारक, शिक्षाशास्त्री के रूप में नयी पीढ़ी के सामने एक दैदीप्यमान सूर्य के रूप में उदित होकर आते हैं।
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री वसंत मून, डा. बाबासाहब आंबेडकर सम्रग ग्रंथावली, जो महाराष्ट्र शासन की ओर से प्रकाशित हो रही है, के प्रधान-संपादक हैं। उन्होंने डा. आंबेडकर की अंग्रेजी में लिखी हुई अनेक पुस्तकों का मराठी में अनुवाद भी किया है। दलित समस्या पर उनकी कई किताबें उपलब्ध हैं। संप्रति वह महाराष्ट्र शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री वसंत मून, डा. बाबासाहब आंबेडकर सम्रग ग्रंथावली, जो महाराष्ट्र शासन की ओर से प्रकाशित हो रही है, के प्रधान-संपादक हैं। उन्होंने डा. आंबेडकर की अंग्रेजी में लिखी हुई अनेक पुस्तकों का मराठी में अनुवाद भी किया है। दलित समस्या पर उनकी कई किताबें उपलब्ध हैं। संप्रति वह महाराष्ट्र शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं।
1
व्यक्ति का जन्म उसके वश की बात नहीं है। उसके पैदा होते ही जाति, वंश और धर्म उससे जुड़ जाते हैं। इनसे उसकी मुक्ति नहीं है। परंतु कर्म ही उसके जीवन को बनाता-बिगाड़ता है। काम करने की योग्यता, उसका कर्म या तो उसे अपशय की खाई में गिराता है या फिर उसे ख्याति के उच्च शिखर पर पहुंचाने का सौभाग्य प्रदान करता है। संसार के महापुरूषों के चरित्रों का अध्ययन करते समय यह बात हमारे ध्यान में अवश्य आती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यह महानता उसे अपने जीवन में त्याग और परिश्रम की भारी पूंजी लगाकर प्राप्त करनी होती है। इसीलिए महाभारत में कर्ण के मुख से जो उक्ति कहलवाई गयी है, यह अत्यंत उपयुक्त है-
दैवायत्तं कुले जन्म
मदायत्तं तु पौरूषम्
मदायत्तं तु पौरूषम्
कर्ण को राधेय कहकर, सूतपुत्र विशेषण से संबोधित कर, अपमानित किया जाता था। किंतु जिस काल में उसका जन्म हुआ उसे भले ही कितना भी हीन घोषित कर दिया गया हो उसमें कर्ण का क्या दोष है ? कर्ण को इसका पूरा बोध था कि अपना पुरूषार्थ दिखाना तो उसके हाथ की बात है। इसीलिए जब भी दानशीलता और पुरूषार्थ की पराकाष्ठा की उपमा देनी हो तो कर्ण को ही याद किया जाता है। अमेरिका और रूस विश्व के दो शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों देशों के प्रमुख निर्माताओ के रूप में रूस के एक समय के सर्वेसर्वा स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहन लिंकन का नाम लेना पड़ता है ये दोनों ही महापुरूष एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे। स्टालिन का जन्म एक चर्मकार के घर में हुआ था। लिंकन भी एक फलों के बाग में बागवानी करने वाली एक जारज महिला की संतान थे। किंतु इन दोनों व्यक्तियों के विकास में सामाजिक गुलामी की बेड़ियों ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। बाबासाहब आंबेडकर अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति में पैदा हुए थे। इसलिए उनके लिए जन्म से ही सामाजिक वातावरण लिंकन और स्टालिन से विपरीत था। फिर भी उन्होंने इस देश के जनजीवन में जो क्रांति पैदा की, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसे अद्वितीय ही कहना होगा।
अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों को एकता के सूत्र में बांधकर—वहां के काले और गोरों के भेद को सबसे पहले समाप्त किया और अमेरिका में प्रथम बार लोकतांत्रिक राज्य-प्रणाली की नींव डाली। उसके विपरीत स्टालिन ने व्यक्ति स्वातंत्र्य का विरोध कर सारे राज्य में समाज सत्तावादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। डा. आंबेडकर ने प्रजातंत्र और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास किया। उन्होंने हजारों वर्षो से हिंदू धर्म द्वारा मान्य अस्पृश्यता को कानून के बल पर नष्ट करवाया। उन्होंने इस देश में जन-जन में निर्माण किये गये भेदों को मिटाकर समान अधिकारों को स्थापित करने वाला संविधान प्रदान किया और ढाई हजार बरसों के बाद पहली बार प्रजातंत्र के मूल्यों की नींव रखी। ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी डा. आंबेडकर का जीवन जितना रोमहर्षक और संघर्षमय है उतना ही वह शिक्षाप्रद भी है।
डा. बाबासाहब आंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी आंबेडकर। उनका पैतृक स्थान रत्नागिरी जिले के मंडणगड तहसील में एक छोटा-सा ग्राम आंबवडे है। भीमराव की माता का नामा था भीमाबाई और पिताजी रामजी वल्द मालोजी सकपाल। महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, प्रभावशाली, अस्पृश्य कहलाये जाने वाली महार जाति में उन्होंने जन्म लिया था।
भीमराव के दादा मालोजी सेना में हवलदार के ओहदे तक पहुंचे थे। परिवार के लडके-लडकियों के लिए दिन में पाठशाला लगती थी और प्रौढ़ लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थीं। इस पाठशाला में रामजी सूबेदार ने प्रधान-अध्यापक के रूप में घनिष्टता हुई और मुरबाडकर ने अपनी कन्या भीमाबाई का विवाह रामजी के साथ संपन्न करवाया।
भीमाबाई संपन्न धनी परिवार में पली थीं। परंतु रामजी को पुणे शहर में शिक्षक-प्रशिक्षण केंद्र में, शिक्षक का काम करते समय बहुत कम वेतन मिलता था। उसमें से कुछ ही रकम वे भीमाबाई को मुंबई भिजवा सकते थे। इसलिए भीमाबाई ने बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में दिन बिताये। सन् 1890 तक रामजी को तेरह संतानें हुई।
जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्यप्रदेश स्थित महू की छावनी में थी तब 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। परिवारजन उसे ‘भीवा’ कहकर पुकारा करते थे। एक दो साल बाद रामजी सेना से सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने रत्नागिरी तहसील में कापदापोली गांव में अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए प्रस्थान किया।
सन् 1894 के आसपास दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अस्पृश्य विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध था। उसके विरूद्ध अस्पृश्य पेंशनरों ने जिलाधीश के पास अर्जी पेश की। अपनी अर्जी में रामजी सूबेदार ने अपने रहने के लिए जगह की भी मांग की। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि दापोली में अपने बच्चों को पाठशाला में भर्ती करना संभव नहीं है तो रामजी सूबेदार अपने परिवार सहित मुंबई में आ बसे। वहां से उन्होंने सेना के अधिकारियों को निवेदनपत्र भेजे और फलस्वरूप सातारा पी. डब्लू. डी. के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी प्राप्त की। सातारा की फौज छावनी में बसे कोंकणवासी महार पेंशनर परिवारों के साथ रहते हुए भीम का बचपन बीता। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई।
बचपन में भीम बहुत ही शरारती था। पास के वटवृक्ष पर रोज ही ‘सूरपारब्या’ खेल खेलने और झगड़े मोल लेने, मारपीट करने, ऊधम मचाने और बखेड़े खड़े करने के मारे, घर के लोगों को भी भीम के इन झमेलों को सुलझाते-सुलझाते मुसीबत हो जाती थी। जब भीम छह साल का हुआ तो मां की मृत्यु हो जाने से वह ममता की छत्रछाया से वंचित हो गया। उसके बाद अपंग बुआ मीराबाई ने ही भीम का लालन पालन किया।
सूबेदार रामजी कबीरपंथी थे। वे रोज अपने बच्चों से भजन, अभंग और दोहों का पाठ करवाते थे। सुबह उठकर वे बच्चों से उनका अभ्यास करवा लेते, इसलिए भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की भी गहरी छाप पड़ी थी।
भीमराव के अस्रृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले कुछ अध्यापक भी थे। आंबेडकर उपनाम वाले एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना कुल-नाम ही नहीं दिया, बल्कि दोपहर की छुट्टी में वे भीमराव को खाने के लिए रोटियां भी दिया करते थे। सन् 1927 के करीब जब आंबेडकर मास्टर उनसे मिलने आये तो बाबासाहब उन्हें देखकर गदगद हो गये, उनका गला भर आया। बाबासाहब ने बहुत दिनों तक मास्टर साहब का प्रेम से ओतप्रोत एक पत्र अपने पास संभाल कर रखा था।
7 नवंबर 1900 के दिन भीवा को वहां के हाईस्कूल में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश मिला। एक दिन पाठशाला से छुट्टी पाने के लिए भीवा बरसात में भीगता हुआ स्कूल पहुंचा। पेंडसे नामक शिक्षक महोदय ने उसे अपने घर भिजवाकर पहनने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए अंगोछा दिलवाया और उसे कक्षा में बैठने का आदेश दिया। उस दिन भीवा ने अपने स्वभाव के हठीलेपन को तिलांजलि देने का निश्चय किया, परंतु उसके जीवन की घटनाओं से यह प्रतीत नहीं होता कि स्वभाव के हठीपन ने हार मान ली हो।
बचपन में भीवा को सातारा में रहते हुए अस्पृश्यता के प्रहारों को सहन करना पड़ता था। उसके सिर के बाल काटने के लिए कोई हज्जाम तैयार नहीं होता था। इसलिए उसकी बड़ी बहन ही उसकी हजामत बनाया करता थी। अकाल के दिनों में रामजी सूबेदार को गोरेगांव के पास काम पर तैनात किया गया था। उनके बच्चे सातारा में रहते थे। एक बार भीम ने अपने बड़े भाई और भांजों को साथ लेकर रेलगाड़ी से गोरेगांव पहुंचा। मगर स्टेशन से गांव तक पहुंचने के लिए उसे और साथियों को, अछूत होने के कारण कोई गाड़ीवान अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर एक बैलगाड़ी वाला मान गया मगर बैलगाड़ी भीम को हांकनी पड़ी। गाड़ीवान गाड़ी पर विराजमान अवश्य था, लेकिन अस्पृश्य के लिए गाड़ी हांकना उसको आन के खिलाफ लग रहा था। किसी को भी इन बच्चों पर दया नहीं आयी, उन्हें डेढ़ दिन बिना पानी के गुजारा करना पड़ा, क्योंकि अछूत होने के कारण उन्हें किसी भी कुएं से पानी पीने को न मिल सका। दूसरे दिन भीम और उनके साथी भूखे-प्यासे अधमरे से अपने गंतव्य तक पहुंचे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैकबोर्ड पर रेखा-गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर उस ब्लैकबोर्ड के पास रखे अपने खाने के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वे अपवित्र न हो जाएं और उसके बाद ही भीम उस सूत्र को ब्लैकबोर्ड पर सिद्ध कर सका। इस प्रकार की अपमानजनक घटनाओं से भीम का मन विद्रोह करने के लिए उद्यत हो उठा था। सन् 1904 में भीवा के चौथी अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण होते ही सूबेदार रामजी अपने परिवार को मुंबई ले गये और परेल मौहल्ले में डबक चाल में घर लेकर वहां पहले से बसे हुए कोंकणवासी महार परिवार के साथ रहने लगे। भीवा को सरकारी एल्फिंस्टन हाईस्कूल में नवम वर्ग में भरती करवा दिया।
इस बीच रामजी ने दूसरा विवाह किया। भीवा को अपनी माता के आभूषण सौतेली मां के शरीर पर देखकर बहुत ही रोष हुआ। तब से उसका मन घर से खट्टा होने लगा और एक दिन जीवन से विरक्त होकर सिद्धार्थ की तरह वह घर छोड़कर चला भी गया। मगर फिर उसे अपने जीवन के लक्ष्य की अभिज्ञता का बोध हुआ और वह जल्द ही घर वापिस लौट आया। जब वह लौटा तो अपने सब आत्मीय जनों, नाते-रिश्तेदारों के चितांतुर चेहरों और डब़डबाई आंखों को देखना उसके लिए असहनीय हो गया।
जैसे-जैसे वह ऊपरी कक्षाओं में प्रवेश कर रहा था, उसके स्वभाव का हठीलापन, उतावलापन और शरारतीपन कम होने लगा और वह अध्ययन की और ध्यान देने लगा। पाठशाला के छूटते ही वह चर्नीरोड गार्डन में जाकर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। उसी उद्यान में कृ. अ. केलूसकर गुरूजी भी संध्या समय पधारा करते तथा अपने अध्ययन में लीन रहते। एक दिन उन्होंने भीम से पूछताछ की और उसे पठन-पाठन के लिए पुस्तकों के चयन का मार्गदर्शन किया।
एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढते समय ही उसके पिता रामजी सूबेदार ने भीवा की शादी भिकू वलंगकर की पुत्री रमाबाई के साथ संपन्न की। विवाह के समय रमा की उम्र 9-10 साल थी और भीवा 17 साल का था।
उन दिनों मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी। अस्पृश्य छात्रों में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला भीमराव पहला विद्यार्थी था। डबक की चाल के निवासियों ने उसका अभिनंदन करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। इस सत्कार समारोह में केलूसकर गुरूजी ने मराठी में स्वरचित भगवान बुद्ध के आत्मचरित्र की पुस्तक भीवा को पुरस्कार के रूप में भेंट की। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे उसकी आगामी शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। उन्होंने इसके बाद भीमराव की बड़ौदा नरेश से भेंट भी करवा दी। श्रीमंत गायकवाड़ ने 20 रूपये माहवार की छात्रवृत्ति भी स्वीकृत कर दी।
3 जनवरी 1908 के दिन भीवा को एल्फिंस्टन कालेज में प्रवेश मिल गया। अब उसे अपनी जिम्मेदारी का बोध होने लगा था और उसका मन खेल में कम ही लगता था। उसने शेक्सपियर के नाटक ‘किंग लियर’ पर ‘शहाणी मुलगी’ नाम का एक प्रहसन भी एक बार प्रस्तुत किया था। संध्या समय वह क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता था। परीक्षा के दिनों में, उसके पिताजी आधी रात में दो बजे उसे नींद से जगाकर पढ़ाई करने के लिए बैठा देते थे, जिससे उसका अध्ययन अच्छी तरह से हो सके। भीवा की पुस्तकों की इच्छा पूरी करने के लिए वे कभी कभी अपनी बिटिया के घर जाकर उसके गहने गिरवी रख देते थे।
उन दिनों एल्फिंस्टन कालेज में धनी और उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। भीवा को अंग्रेजी और फारसी पर अच्छी प्रवीणता थी। इसलिए फारसी के उप-आचार्य के. वी. इरानी और अंग्रेजी के आचार्य प्रो. मुल्लर भीवा पर अधिक स्नेह रखते थे। प्रो. मुल्लर भीवा से इतना प्रेम करते थे कि उसे अपनी शर्ट भी दे दिया करते थे। उन दिनों एल्फिंस्टन कालेज में प्रो. ओसवाल्ड, मुल्लर, जार्ज अंडरसन, प्रिंसिपल कॉवर्नटन जैसे प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। फिर भी भीवा के अंतकरण में नयी चेतना के निर्माण न हो सका, यह बात उतनी ही सच है। बाबासाहब के शब्दों में :‘‘यद्यपि मैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हर साल सफल होता रहा, फिर भी कभी दूसरी श्रेणी नहीं मिली। बी. ए. की परीक्षा में तो मेरी दूसरी श्रेणी कुछ ही अंकों के कारण मिलना रह गई।’’1
उस समय अस्पृश्य समाज की दयनीय स्थिति और शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता पर यदि गौर किया जाये तो रामजी सूबेदार ने जिस लगन और उत्साह के साथ भीवा को बी. ए. तक पढ़ाया वह सचमुच प्रशंसनीय है। सन् 1912 के नबंबर मास में भीवा बी. ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।
उसे 750 अंकों में से 280 अंक मिले। सब बेहद खुश हुए। उसकी पढ़ाई पर पिताजी ने जो अथक परिश्रम किया और जी जान से कोशिश कर खर्च का असहनीय भार भी वहन किया, उसके लिए बाबासाहब ने उनके बाद अपने पिताजी के प्रति अनेकों बार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है।
भीमराव आंबेडकर को कालेज में जो प्राप्तांक पत्र2 मिला उसे यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि उनकी कभी भी पहली श्रेणी के विद्यार्थियों में गणना संभव न थी। किंतु केवल कालेज की शिक्षा ही इंसान की किस्मत का आइना नहीं है। यदि बी. ए. की स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पत्र के आधार पर किसी ने यह भविष्यवाणी की होती कि यह भीमराव आंबेडकर नाम का विद्यार्थी जग-प्रसिद्ध विद्वान होगा, नाम
1. भीवा ने प्रिंसिपल को यह सूचित किया था कि गणित विषय में मैं कमजोर होने के कारण इस नवंबर 1980 की परीक्षा में नहीं बैठूँगा। इस कारण उसका एक साल व्यर्थ गया। (कालेज रिकार्ड)
2. सन् 1909 में प्रीवियस के तेरह उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 884 अंकों में 282 अंक प्राप्त हुए। सन् 1910 की इंटरमीडियेट परीक्षा में भीमराव की विषयानुसार अंक-सूची निम्न प्रकार से हैः—
अंग्रेजी फारसी गणित तर्कशास्त्र
कुलअंक 200 100 200 100
उत्तीर्ण होने के
लिए आवश्यक अंक 60 30 60 30
प्राप्त अंक 69 52 60 42
(एल्फिंस्टन कॉलेज रिकार्ड फाइल्स में)
कुल=223/600
कमाएगा तो उसे पागल करार दिया जाता। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और निपुणता को विस्तृत क्षेत्र मिलता है तो वह किस प्रकार खिल उठता है, इसका अंदाजा भीमराव के भावी जीवन से दृष्टिगोचर होता है।
बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भीमराव ने अपने पिता की इच्छा के विरूद्ध नौकरी करने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ौदा रियासत में प्रार्थना पत्र भेजा। उत्तर में तुरंत ही बड़ौदा रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त कर कार्य ग्रहण करने का आदेश मिला। उन्हें वहां काम पर लगे लगभग 15 दिन ही हो पाये थे कि जनवरी 1913 में उन्हें अपने पिता की गंभीर बीमारी की सूचना तार से मिली। वे तुरंत ही बड़ौदा से रेलगाड़ी द्वारा रवाना हुए। मार्ग में सूरत स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वे परिवार को देने के लिए मिठाई खरीदने गाड़ी से उतरे। इतने में ही गाड़ी चल दी और वे दूसरे दिन मुंबई पहुंच पाये। घर आने पर उन्हें मृत्यु-शैया पर पड़े अपने पिता के दर्शन हुए। ऐसा लगा मानो उनके पिता के प्राणपखेरू अपने बेटे को देखने के लिए रुके हुए थे। 2 फरवरी, 1913 को रामजी सूबेदार का देहावसान हो गया।
रामजी सूबेदार की मृत्यु के बाद भीमराव को अब अपने पैरों पर खड़े रहना आवश्यक हो गया था। किंतु वे अब अपनी नौकरी पर बड़ौदा नहीं जाना चाहते थे। इन्हीं दिनों बड़ौदा नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भिजवाने का निश्चय किया। भीमराव ने नरेश को मुंबई स्थित राजवाड़े में उनसे भेंट की। महाराज ने प्रार्थना पत्र भेजने को कहा और 4 जून, 1913 के दिन भीमराव को बड़ौदा जाकर शिक्षा उपमंत्री के कार्यालय में संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस कारनामे के अनुसार अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण होते ही भीमराव को 10 वर्षों के लिए बड़ौदा राज्य की नौकरी में रहना आवश्यक था।
इसके बाद भीमराव ने तुरंत अमेरिका जाने की तैयारी की। बाइस वर्ष के एक अस्पृश्य युवक को अमेरिका जैसे उन्नत देश में ऊंची पढा़ई का अवसर मिले, यह अपने में ही एक अलभ्य उपलब्धि थी। विश्व में जहां उच्चतर विद्यापीठ हैं, उच्चतम गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, ऐसे देश के महान विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने भारत देश का एक निर्धन-सा विद्यार्थी जा रहा है।1 शिक्षाविद् अमरनाथ झा ने उस समय यह कहा था।
जुलाई की बारह तारीख को आंबेडकर न्यूयार्क पहुंचे। उन्होंने अपने प्रसव में
1.बधौना रामचन्द्रः आंबेडकर का जीवन संघर्ष, पृ.19
अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ रखे थे।1 वे कुछ ही दिन कोलंबिया विद्यापीठ के हार्टले हॉल नामक छात्रावास में रहे। फिर वे 554 वेस्ट, मार्ग 144 स्थित कास्माँपालिटन क्लब में भारतीय विद्यार्थियों के साथ रहने गये। इसके बाद वे नवल भतना नामक एक पारसी विद्यार्थी के साथ लिविंगस्टन हॉल के छात्रावास में रहने लगे।
श्री भतना के साथ उनकी यह मित्रता जीवन भर कायम रही। वैसे अमेरिका में उनके एकमात्र मित्र सी. एस. देवल थे जिनके साथ वे घंटों चर्चा किया करते थे।2
1. बनौधा रामचन्द्र : आंबडेकर का जीवन संघर्ष, पृ. 17
2. बनौधा, रामचन्द्र : पृ. 17
अन्य चरित्र ग्रंथों में श्री देवल का उल्लेख नहीं है। किंतु बनौधा को दी हुई जानकारी स्वयं डा. आंबेडकर ने उन्हें बताई, यह बनौधा ने लिखा है।
अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों को एकता के सूत्र में बांधकर—वहां के काले और गोरों के भेद को सबसे पहले समाप्त किया और अमेरिका में प्रथम बार लोकतांत्रिक राज्य-प्रणाली की नींव डाली। उसके विपरीत स्टालिन ने व्यक्ति स्वातंत्र्य का विरोध कर सारे राज्य में समाज सत्तावादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। डा. आंबेडकर ने प्रजातंत्र और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने का स्वप्न साकार करने का प्रयास किया। उन्होंने हजारों वर्षो से हिंदू धर्म द्वारा मान्य अस्पृश्यता को कानून के बल पर नष्ट करवाया। उन्होंने इस देश में जन-जन में निर्माण किये गये भेदों को मिटाकर समान अधिकारों को स्थापित करने वाला संविधान प्रदान किया और ढाई हजार बरसों के बाद पहली बार प्रजातंत्र के मूल्यों की नींव रखी। ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी डा. आंबेडकर का जीवन जितना रोमहर्षक और संघर्षमय है उतना ही वह शिक्षाप्रद भी है।
डा. बाबासाहब आंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी आंबेडकर। उनका पैतृक स्थान रत्नागिरी जिले के मंडणगड तहसील में एक छोटा-सा ग्राम आंबवडे है। भीमराव की माता का नामा था भीमाबाई और पिताजी रामजी वल्द मालोजी सकपाल। महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, प्रभावशाली, अस्पृश्य कहलाये जाने वाली महार जाति में उन्होंने जन्म लिया था।
भीमराव के दादा मालोजी सेना में हवलदार के ओहदे तक पहुंचे थे। परिवार के लडके-लडकियों के लिए दिन में पाठशाला लगती थी और प्रौढ़ लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थीं। इस पाठशाला में रामजी सूबेदार ने प्रधान-अध्यापक के रूप में घनिष्टता हुई और मुरबाडकर ने अपनी कन्या भीमाबाई का विवाह रामजी के साथ संपन्न करवाया।
भीमाबाई संपन्न धनी परिवार में पली थीं। परंतु रामजी को पुणे शहर में शिक्षक-प्रशिक्षण केंद्र में, शिक्षक का काम करते समय बहुत कम वेतन मिलता था। उसमें से कुछ ही रकम वे भीमाबाई को मुंबई भिजवा सकते थे। इसलिए भीमाबाई ने बहुत ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में दिन बिताये। सन् 1890 तक रामजी को तेरह संतानें हुई।
जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्यप्रदेश स्थित महू की छावनी में थी तब 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। परिवारजन उसे ‘भीवा’ कहकर पुकारा करते थे। एक दो साल बाद रामजी सेना से सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने रत्नागिरी तहसील में कापदापोली गांव में अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए प्रस्थान किया।
सन् 1894 के आसपास दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अस्पृश्य विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध था। उसके विरूद्ध अस्पृश्य पेंशनरों ने जिलाधीश के पास अर्जी पेश की। अपनी अर्जी में रामजी सूबेदार ने अपने रहने के लिए जगह की भी मांग की। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि दापोली में अपने बच्चों को पाठशाला में भर्ती करना संभव नहीं है तो रामजी सूबेदार अपने परिवार सहित मुंबई में आ बसे। वहां से उन्होंने सेना के अधिकारियों को निवेदनपत्र भेजे और फलस्वरूप सातारा पी. डब्लू. डी. के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी प्राप्त की। सातारा की फौज छावनी में बसे कोंकणवासी महार पेंशनर परिवारों के साथ रहते हुए भीम का बचपन बीता। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई।
बचपन में भीम बहुत ही शरारती था। पास के वटवृक्ष पर रोज ही ‘सूरपारब्या’ खेल खेलने और झगड़े मोल लेने, मारपीट करने, ऊधम मचाने और बखेड़े खड़े करने के मारे, घर के लोगों को भी भीम के इन झमेलों को सुलझाते-सुलझाते मुसीबत हो जाती थी। जब भीम छह साल का हुआ तो मां की मृत्यु हो जाने से वह ममता की छत्रछाया से वंचित हो गया। उसके बाद अपंग बुआ मीराबाई ने ही भीम का लालन पालन किया।
सूबेदार रामजी कबीरपंथी थे। वे रोज अपने बच्चों से भजन, अभंग और दोहों का पाठ करवाते थे। सुबह उठकर वे बच्चों से उनका अभ्यास करवा लेते, इसलिए भीमराव के मन पर धार्मिक शिक्षा के संस्कारों की भी गहरी छाप पड़ी थी।
भीमराव के अस्रृश्य होते हुए भी उनके प्रति स्नेह रखने वाले कुछ अध्यापक भी थे। आंबेडकर उपनाम वाले एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अपना कुल-नाम ही नहीं दिया, बल्कि दोपहर की छुट्टी में वे भीमराव को खाने के लिए रोटियां भी दिया करते थे। सन् 1927 के करीब जब आंबेडकर मास्टर उनसे मिलने आये तो बाबासाहब उन्हें देखकर गदगद हो गये, उनका गला भर आया। बाबासाहब ने बहुत दिनों तक मास्टर साहब का प्रेम से ओतप्रोत एक पत्र अपने पास संभाल कर रखा था।
7 नवंबर 1900 के दिन भीवा को वहां के हाईस्कूल में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश मिला। एक दिन पाठशाला से छुट्टी पाने के लिए भीवा बरसात में भीगता हुआ स्कूल पहुंचा। पेंडसे नामक शिक्षक महोदय ने उसे अपने घर भिजवाकर पहनने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के लिए अंगोछा दिलवाया और उसे कक्षा में बैठने का आदेश दिया। उस दिन भीवा ने अपने स्वभाव के हठीलेपन को तिलांजलि देने का निश्चय किया, परंतु उसके जीवन की घटनाओं से यह प्रतीत नहीं होता कि स्वभाव के हठीपन ने हार मान ली हो।
बचपन में भीवा को सातारा में रहते हुए अस्पृश्यता के प्रहारों को सहन करना पड़ता था। उसके सिर के बाल काटने के लिए कोई हज्जाम तैयार नहीं होता था। इसलिए उसकी बड़ी बहन ही उसकी हजामत बनाया करता थी। अकाल के दिनों में रामजी सूबेदार को गोरेगांव के पास काम पर तैनात किया गया था। उनके बच्चे सातारा में रहते थे। एक बार भीम ने अपने बड़े भाई और भांजों को साथ लेकर रेलगाड़ी से गोरेगांव पहुंचा। मगर स्टेशन से गांव तक पहुंचने के लिए उसे और साथियों को, अछूत होने के कारण कोई गाड़ीवान अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर एक बैलगाड़ी वाला मान गया मगर बैलगाड़ी भीम को हांकनी पड़ी। गाड़ीवान गाड़ी पर विराजमान अवश्य था, लेकिन अस्पृश्य के लिए गाड़ी हांकना उसको आन के खिलाफ लग रहा था। किसी को भी इन बच्चों पर दया नहीं आयी, उन्हें डेढ़ दिन बिना पानी के गुजारा करना पड़ा, क्योंकि अछूत होने के कारण उन्हें किसी भी कुएं से पानी पीने को न मिल सका। दूसरे दिन भीम और उनके साथी भूखे-प्यासे अधमरे से अपने गंतव्य तक पहुंचे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैकबोर्ड पर रेखा-गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर उस ब्लैकबोर्ड के पास रखे अपने खाने के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वे अपवित्र न हो जाएं और उसके बाद ही भीम उस सूत्र को ब्लैकबोर्ड पर सिद्ध कर सका। इस प्रकार की अपमानजनक घटनाओं से भीम का मन विद्रोह करने के लिए उद्यत हो उठा था। सन् 1904 में भीवा के चौथी अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण होते ही सूबेदार रामजी अपने परिवार को मुंबई ले गये और परेल मौहल्ले में डबक चाल में घर लेकर वहां पहले से बसे हुए कोंकणवासी महार परिवार के साथ रहने लगे। भीवा को सरकारी एल्फिंस्टन हाईस्कूल में नवम वर्ग में भरती करवा दिया।
इस बीच रामजी ने दूसरा विवाह किया। भीवा को अपनी माता के आभूषण सौतेली मां के शरीर पर देखकर बहुत ही रोष हुआ। तब से उसका मन घर से खट्टा होने लगा और एक दिन जीवन से विरक्त होकर सिद्धार्थ की तरह वह घर छोड़कर चला भी गया। मगर फिर उसे अपने जीवन के लक्ष्य की अभिज्ञता का बोध हुआ और वह जल्द ही घर वापिस लौट आया। जब वह लौटा तो अपने सब आत्मीय जनों, नाते-रिश्तेदारों के चितांतुर चेहरों और डब़डबाई आंखों को देखना उसके लिए असहनीय हो गया।
जैसे-जैसे वह ऊपरी कक्षाओं में प्रवेश कर रहा था, उसके स्वभाव का हठीलापन, उतावलापन और शरारतीपन कम होने लगा और वह अध्ययन की और ध्यान देने लगा। पाठशाला के छूटते ही वह चर्नीरोड गार्डन में जाकर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अध्ययन करता रहता था। उसी उद्यान में कृ. अ. केलूसकर गुरूजी भी संध्या समय पधारा करते तथा अपने अध्ययन में लीन रहते। एक दिन उन्होंने भीम से पूछताछ की और उसे पठन-पाठन के लिए पुस्तकों के चयन का मार्गदर्शन किया।
एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढते समय ही उसके पिता रामजी सूबेदार ने भीवा की शादी भिकू वलंगकर की पुत्री रमाबाई के साथ संपन्न की। विवाह के समय रमा की उम्र 9-10 साल थी और भीवा 17 साल का था।
उन दिनों मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती थी। अस्पृश्य छात्रों में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला भीमराव पहला विद्यार्थी था। डबक की चाल के निवासियों ने उसका अभिनंदन करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। इस सत्कार समारोह में केलूसकर गुरूजी ने मराठी में स्वरचित भगवान बुद्ध के आत्मचरित्र की पुस्तक भीवा को पुरस्कार के रूप में भेंट की। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे उसकी आगामी शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। उन्होंने इसके बाद भीमराव की बड़ौदा नरेश से भेंट भी करवा दी। श्रीमंत गायकवाड़ ने 20 रूपये माहवार की छात्रवृत्ति भी स्वीकृत कर दी।
3 जनवरी 1908 के दिन भीवा को एल्फिंस्टन कालेज में प्रवेश मिल गया। अब उसे अपनी जिम्मेदारी का बोध होने लगा था और उसका मन खेल में कम ही लगता था। उसने शेक्सपियर के नाटक ‘किंग लियर’ पर ‘शहाणी मुलगी’ नाम का एक प्रहसन भी एक बार प्रस्तुत किया था। संध्या समय वह क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता था। परीक्षा के दिनों में, उसके पिताजी आधी रात में दो बजे उसे नींद से जगाकर पढ़ाई करने के लिए बैठा देते थे, जिससे उसका अध्ययन अच्छी तरह से हो सके। भीवा की पुस्तकों की इच्छा पूरी करने के लिए वे कभी कभी अपनी बिटिया के घर जाकर उसके गहने गिरवी रख देते थे।
उन दिनों एल्फिंस्टन कालेज में धनी और उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। भीवा को अंग्रेजी और फारसी पर अच्छी प्रवीणता थी। इसलिए फारसी के उप-आचार्य के. वी. इरानी और अंग्रेजी के आचार्य प्रो. मुल्लर भीवा पर अधिक स्नेह रखते थे। प्रो. मुल्लर भीवा से इतना प्रेम करते थे कि उसे अपनी शर्ट भी दे दिया करते थे। उन दिनों एल्फिंस्टन कालेज में प्रो. ओसवाल्ड, मुल्लर, जार्ज अंडरसन, प्रिंसिपल कॉवर्नटन जैसे प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। फिर भी भीवा के अंतकरण में नयी चेतना के निर्माण न हो सका, यह बात उतनी ही सच है। बाबासाहब के शब्दों में :‘‘यद्यपि मैं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हर साल सफल होता रहा, फिर भी कभी दूसरी श्रेणी नहीं मिली। बी. ए. की परीक्षा में तो मेरी दूसरी श्रेणी कुछ ही अंकों के कारण मिलना रह गई।’’1
उस समय अस्पृश्य समाज की दयनीय स्थिति और शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता पर यदि गौर किया जाये तो रामजी सूबेदार ने जिस लगन और उत्साह के साथ भीवा को बी. ए. तक पढ़ाया वह सचमुच प्रशंसनीय है। सन् 1912 के नबंबर मास में भीवा बी. ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।
उसे 750 अंकों में से 280 अंक मिले। सब बेहद खुश हुए। उसकी पढ़ाई पर पिताजी ने जो अथक परिश्रम किया और जी जान से कोशिश कर खर्च का असहनीय भार भी वहन किया, उसके लिए बाबासाहब ने उनके बाद अपने पिताजी के प्रति अनेकों बार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है।
भीमराव आंबेडकर को कालेज में जो प्राप्तांक पत्र2 मिला उसे यदि देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि उनकी कभी भी पहली श्रेणी के विद्यार्थियों में गणना संभव न थी। किंतु केवल कालेज की शिक्षा ही इंसान की किस्मत का आइना नहीं है। यदि बी. ए. की स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पत्र के आधार पर किसी ने यह भविष्यवाणी की होती कि यह भीमराव आंबेडकर नाम का विद्यार्थी जग-प्रसिद्ध विद्वान होगा, नाम
1. भीवा ने प्रिंसिपल को यह सूचित किया था कि गणित विषय में मैं कमजोर होने के कारण इस नवंबर 1980 की परीक्षा में नहीं बैठूँगा। इस कारण उसका एक साल व्यर्थ गया। (कालेज रिकार्ड)
2. सन् 1909 में प्रीवियस के तेरह उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 884 अंकों में 282 अंक प्राप्त हुए। सन् 1910 की इंटरमीडियेट परीक्षा में भीमराव की विषयानुसार अंक-सूची निम्न प्रकार से हैः—
अंग्रेजी फारसी गणित तर्कशास्त्र
कुलअंक 200 100 200 100
उत्तीर्ण होने के
लिए आवश्यक अंक 60 30 60 30
प्राप्त अंक 69 52 60 42
(एल्फिंस्टन कॉलेज रिकार्ड फाइल्स में)
कुल=223/600
कमाएगा तो उसे पागल करार दिया जाता। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और निपुणता को विस्तृत क्षेत्र मिलता है तो वह किस प्रकार खिल उठता है, इसका अंदाजा भीमराव के भावी जीवन से दृष्टिगोचर होता है।
बी. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भीमराव ने अपने पिता की इच्छा के विरूद्ध नौकरी करने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ौदा रियासत में प्रार्थना पत्र भेजा। उत्तर में तुरंत ही बड़ौदा रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त कर कार्य ग्रहण करने का आदेश मिला। उन्हें वहां काम पर लगे लगभग 15 दिन ही हो पाये थे कि जनवरी 1913 में उन्हें अपने पिता की गंभीर बीमारी की सूचना तार से मिली। वे तुरंत ही बड़ौदा से रेलगाड़ी द्वारा रवाना हुए। मार्ग में सूरत स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वे परिवार को देने के लिए मिठाई खरीदने गाड़ी से उतरे। इतने में ही गाड़ी चल दी और वे दूसरे दिन मुंबई पहुंच पाये। घर आने पर उन्हें मृत्यु-शैया पर पड़े अपने पिता के दर्शन हुए। ऐसा लगा मानो उनके पिता के प्राणपखेरू अपने बेटे को देखने के लिए रुके हुए थे। 2 फरवरी, 1913 को रामजी सूबेदार का देहावसान हो गया।
रामजी सूबेदार की मृत्यु के बाद भीमराव को अब अपने पैरों पर खड़े रहना आवश्यक हो गया था। किंतु वे अब अपनी नौकरी पर बड़ौदा नहीं जाना चाहते थे। इन्हीं दिनों बड़ौदा नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भिजवाने का निश्चय किया। भीमराव ने नरेश को मुंबई स्थित राजवाड़े में उनसे भेंट की। महाराज ने प्रार्थना पत्र भेजने को कहा और 4 जून, 1913 के दिन भीमराव को बड़ौदा जाकर शिक्षा उपमंत्री के कार्यालय में संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस कारनामे के अनुसार अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण होते ही भीमराव को 10 वर्षों के लिए बड़ौदा राज्य की नौकरी में रहना आवश्यक था।
इसके बाद भीमराव ने तुरंत अमेरिका जाने की तैयारी की। बाइस वर्ष के एक अस्पृश्य युवक को अमेरिका जैसे उन्नत देश में ऊंची पढा़ई का अवसर मिले, यह अपने में ही एक अलभ्य उपलब्धि थी। विश्व में जहां उच्चतर विद्यापीठ हैं, उच्चतम गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, ऐसे देश के महान विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने भारत देश का एक निर्धन-सा विद्यार्थी जा रहा है।1 शिक्षाविद् अमरनाथ झा ने उस समय यह कहा था।
जुलाई की बारह तारीख को आंबेडकर न्यूयार्क पहुंचे। उन्होंने अपने प्रसव में
1.बधौना रामचन्द्रः आंबेडकर का जीवन संघर्ष, पृ.19
अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ रखे थे।1 वे कुछ ही दिन कोलंबिया विद्यापीठ के हार्टले हॉल नामक छात्रावास में रहे। फिर वे 554 वेस्ट, मार्ग 144 स्थित कास्माँपालिटन क्लब में भारतीय विद्यार्थियों के साथ रहने गये। इसके बाद वे नवल भतना नामक एक पारसी विद्यार्थी के साथ लिविंगस्टन हॉल के छात्रावास में रहने लगे।
श्री भतना के साथ उनकी यह मित्रता जीवन भर कायम रही। वैसे अमेरिका में उनके एकमात्र मित्र सी. एस. देवल थे जिनके साथ वे घंटों चर्चा किया करते थे।2
1. बनौधा रामचन्द्र : आंबडेकर का जीवन संघर्ष, पृ. 17
2. बनौधा, रामचन्द्र : पृ. 17
अन्य चरित्र ग्रंथों में श्री देवल का उल्लेख नहीं है। किंतु बनौधा को दी हुई जानकारी स्वयं डा. आंबेडकर ने उन्हें बताई, यह बनौधा ने लिखा है।
2
जिस समय अन्य विद्यार्थी सिनेमा, शराब और सिगरेट पर पैसा बहाते थे, उन दिनों भीमराव पुस्तकें खरीदने के सिवा अन्य कोई खर्च नहीं करते थे। शराब और सिगरेट को उन्होनें कभी स्पर्श तक नहीं किया था। केवल बचपन से लगी हुई चाय-पान की आदत वहां अवश्य बढ़ गयी थी। उन्हीं दिनों उन्हें अपनी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ा था।
अमेरिका में रहते समय अपने जीवन में उन्हें तत्काल परिवर्तन प्रतीत हुआ। यहां का जीवन उनके मन को नवीन अनुभवों से ओत प्रोत कर रहा था। उनके मन की सीमाएं विस्तृत हो उठीं थी। उनकी ठोस भुजाएँ, गठीला बदन और हष्ट-पुष्ट शरीर देखकर अमेरिकी छात्र उन्हें आदरणीय मानने लगे। जब उन्हें पता चला कि भीमराव भारतीय प्रणाली का व्यायाम करते हैं तो वे उनसे व्यायाम विधि भी सीखने आने लगे।1
इस प्रकार गुरूताप्राप्त में उनकी लेखनी भी प्रौढ़ व्यक्ति के समान उपदेशात्मक पत्र लिखने लगी तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जमेदार नामक व्यक्ति को लिखे गये पत्र में2 उन्होंने शेक्सपियर के नाटक की कुछ पंक्तियां उद्धधृत करते हुए यह दर्शाया कि व्यक्ति के जीवन में अवसरों का समुद्र लहराता है। यदि उन अवसरों का सही प्रयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है।’’ सामाजिक बुराइयों का रोग निदान करते हुए वे कहते हैं, ‘‘माता-पिता अपनी संतान के केवल जन्म दाता हैं, वे उसके भाग्य दाता नहीं है। इस दैवी निधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि संतान का भवितव्य माता-पिता के हाथ में है। बेटों के समान ही अपनी बेटियों को भी लिखाया-पढ़ाया जाये तो हमारा विकास तीव्रगति से हो सकता है, यह निश्चित है।’’ आंबेडकर के इस पत्र में उनका स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मोद्धार के लिए मची हलचल का अंकुर स्पष्ट दिखाई देता है।
1. बनौधा : पृ. 18
2. खैरमोडे : खंड 1 पृ. 66-67—पत्र दिनांक 4-8-1913
अमेरिका में रहते समय अपने जीवन में उन्हें तत्काल परिवर्तन प्रतीत हुआ। यहां का जीवन उनके मन को नवीन अनुभवों से ओत प्रोत कर रहा था। उनके मन की सीमाएं विस्तृत हो उठीं थी। उनकी ठोस भुजाएँ, गठीला बदन और हष्ट-पुष्ट शरीर देखकर अमेरिकी छात्र उन्हें आदरणीय मानने लगे। जब उन्हें पता चला कि भीमराव भारतीय प्रणाली का व्यायाम करते हैं तो वे उनसे व्यायाम विधि भी सीखने आने लगे।1
इस प्रकार गुरूताप्राप्त में उनकी लेखनी भी प्रौढ़ व्यक्ति के समान उपदेशात्मक पत्र लिखने लगी तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जमेदार नामक व्यक्ति को लिखे गये पत्र में2 उन्होंने शेक्सपियर के नाटक की कुछ पंक्तियां उद्धधृत करते हुए यह दर्शाया कि व्यक्ति के जीवन में अवसरों का समुद्र लहराता है। यदि उन अवसरों का सही प्रयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है।’’ सामाजिक बुराइयों का रोग निदान करते हुए वे कहते हैं, ‘‘माता-पिता अपनी संतान के केवल जन्म दाता हैं, वे उसके भाग्य दाता नहीं है। इस दैवी निधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि संतान का भवितव्य माता-पिता के हाथ में है। बेटों के समान ही अपनी बेटियों को भी लिखाया-पढ़ाया जाये तो हमारा विकास तीव्रगति से हो सकता है, यह निश्चित है।’’ आंबेडकर के इस पत्र में उनका स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मोद्धार के लिए मची हलचल का अंकुर स्पष्ट दिखाई देता है।
1. बनौधा : पृ. 18
2. खैरमोडे : खंड 1 पृ. 66-67—पत्र दिनांक 4-8-1913
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book